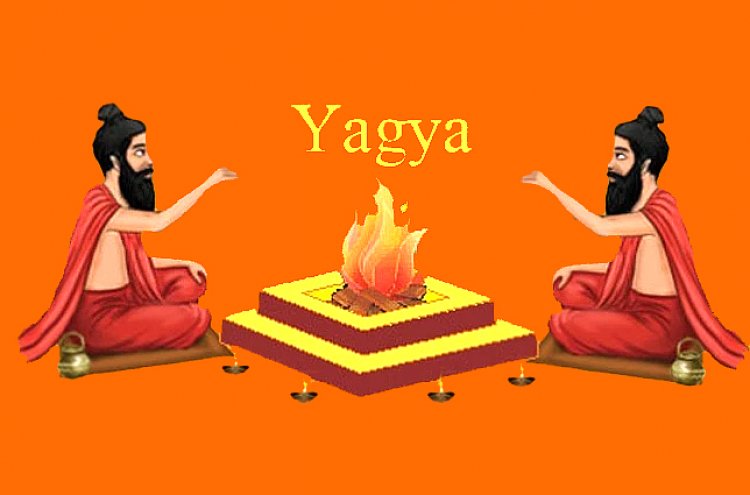
यज्ञ एक विशिष्ट वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जिससे मनुष्य अपने जीवन को सफल बना सकता है। यज्ञ के माध्यम से आध्यात्मिक संपदा की भी प्राप्ति होती है। श्रीमद्भागवत गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने यज्ञ करने वालों को परमगति प्राप्त होने की बात कही है। संत प्रवर विज्ञानदेव जी महाराज कहते हैं यज्ञ भारतीय संस्कृति का प्राण तथा वैदिक धर्म का सार है। यज्ञ ही संसार में श्रेष्ठतम कर्म है। उन्होंने कहा कि यज्ञ को केवल भौतिक कर्मकांड न समझा जाए अपितु इसे आध्यात्मिक रूप से समझकर आध्यात्मिक अनुष्ठान आवश्यक है। वस्तुत: यज्ञ एक आंतरिक प्रक्रिया है, बाह्य यज्ञ उसी का प्रतीक है। भौतिक दृष्टि से यज्ञ का महत्व अत्यधिक है, साथ ही आंतरिक, वैचारिक, मानसिक प्रदूषण समाप्त करने का यह अमोघ उपाय है। वे कहते हैं यज्ञ से भौतिक कामनाओं की पूर्ति तो होती ही है, किंतु यज्ञ की मुख्य भावना का तात्पर्य स्वार्थ का त्याग, परोपकारी जीवन व्यतीत करने से है।
यज्ञ का अर्थ
यज्ञ के तीन प्रमुख अर्थ हैं देव पूजा, दान, और संगठित करना। यज्ञ के तीन ही तात्पर्य हैं-त्याग, बलिदान और शुभ कर्म। सामाजिक प्रगति का सम्पूर्ण आधार सहकारी त्याग, परोपकार आदि प्रवृत्तिओं से है। इस तरह से यज्ञ पूजन के साथ सामाजिक उद्देश्य को पूरा करने की एक प्रक्रिया है। वर्तमान में सर्वशक्तिमान परमात्मा के साथ साझेदारी के सूत्र हैं- उपासना: अपनी चेतना को सांसारिक विषयों से हटा कर परमात्मा की चेतना के निकट ले जाना और उससे भावनात्मक आदान-प्रदान के बाद उससे एक होने का प्रयास करना।
साधना: जीवन को ईश्वरीय अनुशासन के अनुरूप ढालना।
आराधना: इस सुंदर प्रकृति को और अधिक सुंदर बनाने का प्रयास करना सच्ची ईश्वरीय आराधना है। प्रकृति में पशु, पक्षी और वृक्ष सभी आ जाते हैं।
यज्ञ का महत्व
हवन में विशेष प्रकार के पदार्थों की आहुति देने से कई तरह के रोग नष्ट होते हैं। इसे आधुनिक विज्ञान की भाषा में यज्ञ चिकित्सा कहते हैं। कई देशों में यज्ञ चिकित्सा का प्रचलन बढ़ रहा है, जैसे कि टाइफाइड में नीम, चिरायता, त्रिफला और गाय का शुद्ध घी, चावल की आहुति डालने से महत्वपूर्ण गैस जैसे एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड आदि उत्पन्न होती हैं। एथिलीन ऑक्साइड गैस बैक्टीरिया रोधक गैस के रूप में सबसे अधिक उपयोग की जाती है। इसका उपयोग ऑपरेशन से लेकर जीवन रक्षक दवाएं बनाने में भी होता है। प्रोपिलीन ऑक्साइड गैस कृत्रिम वर्षा में मददगार मानी जाती है।
गाय के घी में रेडियो एक्टिव रेडिएशंस के साइड इफेक्ट्स को नष्ट करने की क्षमता है।
अग्नि में गाय के घी की आहुति देने से उसका धुआ जहां तक फैलता है, वहां तक वातावरण प्रदूषण और एटॉमिक रेडिएशन से मुक्त हो जाता है। गाय के घी में कई गुणकारी और चमत्कारी परिणाम मिलते है। यज्ञ में प्रयुक्त समग्री का नकारात्मकता को दूर करने में विशेष महत्व है। इससे पैदा होने वाली गर्मी और राख मानव शरीर और दिमाग को ठीक करती है। यज्ञ के दौरान जब आप अग्नि के सामने बैठते हैं, तो शरीर के विषाक्त पदार्थ निकल जाते हैं।
यज्ञ का उद्देश्य
यज्ञ योग की एक विधि है। यह प्रकृति से जुड़ने की अद्भुत सनातन व्यवस्था है। यज्ञ का प्रमुख उद्देश्य धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों को सद्प्रयोजन के लिए संगठित करना और समूह में एकत्र होकर मंत्र उच्चारण से मन और भाव को केंद्रित करना है। यज्ञ की प्रक्रिया प्रत्यक्ष रूप से अनेक इद्रीय दोष को रोकती है और शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से व्यक्ति को शुद्ध करती है। सनातन व्यवस्था में सामूहिक सामूहिक प्रार्थना को अधिक प्रभावशाली माना गया हैं।
यज्ञ के नियम
यज्ञ शुभ और देव कार्य है। यह शुद्ध होने की प्रक्रिया है। देवता से जोड़ने की पहली शर्त पवित्रता ही है। इसलिए यज्ञ में प्रयोग की जाने वाली हर वस्तु शुद्ध और पवित्र होनी चाहिए। यज्ञ में शामिल होने वालों को भी मन, विचार, तन और व्यवहार से शांत और पवित्र होना चाहिए। ऐसा करके एकाग्र मन से मंत्रों और प्रार्थना द्वारा सर्वशक्तिमान ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करते हैं।
यज्ञ में किसका ध्यान
यज्ञ में सूर्य का ध्यान किया जाता है। सूर्य से सारे विश्व में प्राण का संचार होता है। यह जीवन की ऊर्जा का स्त्रोत है। इस ऊर्जा को प्राणशक्ति भी कहा गया है। वृक्ष, पशु सीमित मात्रा में प्राण शक्ति धारण करते रहते हैं। मनुष्य में यह क्षमता होती है कि वह ध्यान या मेडिटेशन और यज्ञ के द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुरूप बड़ी मात्रा में प्राणशक्ति को धारण कर सकते हैं। इसी कारण शरीर से सामान्य दिखने वाले अनेक महापुरुषों ने असाधारण कार्य किए हैं।
यज्ञ के प्रकार
ब्रह्म यज्ञ:-यह सबसे पहला यज्ञ माना जाता है। ईश्वर को ही ब्रह्म कहा गया है और ब्रह्म यज्ञ उन्हीं को अर्पित होता है। कहा जाता है की यह यज्ञ, नित्य संध्या-वंदन और स्वाध्याय के साथ वेद-पाठ करने से ऋषियों का ऋण चुक जाता है।
देव यज्ञ: घर में होने वाले तमाम यज्ञ को देव यज्ञ की ही श्रेणी में रखा गया है। संधिकाल में गायत्री मंत्र के साथ यह यज्ञ किया जाता है और इससे देव ऋण चुकाया जाता है। इस यज्ञ को संपन्न करने में सात वृक्षों की लकड़ियां लगती हैं, जिनके नाम हैं आम, बड़, पीपल, ढाक, जांटी, जामुन और शमी । इस यज्ञ-हवन से पॉजिटिविटी बढ़ती है, तथा रोग-शोक नष्ट होते हैं।
अश्वमेघ यज्ञ: इस यज्ञ का आयोजन चक्रवर्ती सम्राट बनने के उद्देश्य से किया गया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार, जो सौ बार यह यज्ञ करता है, वह इंद्र का पद प्राप्त करता है।
राजसूर्य यज्ञ: किसी राजा द्वारा यह यज्ञ अपनी कीर्ति और राज्य की सीमाएं बढ़ाने के लिए किया जाता था। इसके अंतर्गत पड़ोसी राज्य से मित्रतापूर्वक व्यवहार द्वारा या फिर युद्ध कर के जबर्दस्ती कर वसूला जाता था।
पितृ यज्ञ: श्रद्धा और सत् भाव के साथ किए गए कर्म, जिनसे माता-पिता और आचार्य तृप्त होते हैं, उसे ही पितृ यज्ञ कहा जाता है। वेदों के अनुसार, श्राद्ध-तर्पण हमारे पूर्वजों को अर्पित किया जाता है। संतान की उत्पत्ति और उनका लाभ धारण करने से पितृ ऋण चुकता होता है, और इसे ही पितृ यज्ञ कहा गया है।
‘भूत’ यज्ञ: हमारा शरीर पांच तत्वों से बना है- पृथ्वी – मृत शरीर को जलाने के लिए भूमि या जमीन पर ही चिता का निर्माण किया जाता है। जल– दाह संस्कार के समय मटके में पानी लेकर चिता की परिक्रमा करते हैं। अग्नि– आग का आशय जलाने से है। वायु– वायु की मदद से ही मृत शरीर के अंतिम अवशेष आकाश की ओर जाते हैं और आकाश – जलने के पश्चात जो राख बचती है वह धुए एवं राख के माध्यम से आकाश में उड़ जाती है।
इन्हीं पांच तत्वों से बने शरीर के लिए यह यज्ञ किया जाता है। भोजन करते समय कुछ अंश अग्नि में डाला जाता है और तत्पश्चात कुछ गाय, कुत्ते और कौवे को दिया जाता है, वेदों, पुराणों में इसे ही भूत यज्ञ कहा गया है।
अतिथि या मनुष्य यज्ञ: घर आए मेहमानों की सेवा करना, अन्न-जल से उनका उचित सेवा-सत्कार करने से जहां ‘अतिथि यज्ञ‘ संपन्न होता है, वहीं जीव ऋण भी उतर जाता है। किसी जरूरतमंद अपंग, महिला, विद्यार्थी, संन्यासी, चिकित्सक और धर्म के रक्षकों की सेवा-सहायता करना भी ‘अतिथि यज्ञ‘ की श्रेणी में आता है। इसे सामाजिक कर्त्तव्य भी माना गया है।
यज्ञ की विधि
परमात्मा की दैवीय शक्तियां विश्व की व्यवस्था को बनाए रखने में लगी रहती है और इसका माध्यम बनती है प्रकृति। हम भी वैदिक काल से लोकमंगल के लिए यज्ञ करते रहे हैं। इसमें देवताओं का आवाहन के साथ प्रकृति की शक्तियों की स्तुतिगान करते हैं। यज्ञ पूजन इस प्रकार से-
कलश स्थापना : सर्वप्रथम कलश स्थापित करते हैं। यहां कलश ब्रह्मांड का प्रतीक है, क्योंकि इसमें धारण करने की क्षमता है। कलश में जल होता है। यहां पर संपूर्ण ब्रह्मांड को केंद्र में रखकर ही पूजन कर रहे हैं अथार्त प्रकृति का ही पूजन करते हैं। हम कामना करते हैं कि कलश में स्थापित देवताओं का कार्य प्रभाव क्षेत्र बढे और निवेदन करते हैं कि उनकी हम पर विशेष कृपा दृष्टि बनी रहे।
शंखनाद: यज्ञ का आवश्यक अंग है शंखनाद। पूजन से पहले यह ध्वनि उत्पन्न की जाती है।
तिलक: यज्ञ में भी किसी पूजा स्तुति या कर्मकांड की तरह माथे पर चंदन धारण करते हैं या तिलक लगाते हैं। तिलक लगाते समय हम प्रार्थना करते हैं कि देव शक्तियां इस चंदन रोली के माध्यम से हमारे मस्तिष्क को सुसंस्कारित बनाएं, विचारों में श्रेष्ठता का भाव बना रहे, मस्तिष्क स्वच्छ और स्वस्थ रहें। इसमें देवत्व का संचार होता रहे।
अग्नि: ऋग्वेद में अग्नि को आराध्य और आदि देव माना गया है। अग्नि की गति ऊपर की ओर होती है। अग्नि स्वयं प्रकाशित है। अग्नि से मिलकर हर पदार्थ अग्नि रूप हो जाता है। अग्नि देव को जो कुछ प्राप्त होता है, वह सब में समान रूप से में वितरित कर देते हैं। अपने लिए बचा कर रखने की प्रवृत्ति अग्नि में नहीं होती।
आसन: यज्ञ के दौरान विशेष अवस्था में बैठने का कारण उसका आसन है, जिसके द्वारा योगासन का लाभ प्राप्त होता है।
आहुति: आहुति देने के लिए विशेष अंगुलियों का प्रयोग किया जाता है। ऐसा करने का एकमात्र कारण है एक्यूप्रेशर का लाभ प्राप्त हो सके।
ध्वनि: सनातन में ध्वनियों का विशेष महत्व है। धर्मशास्त्र ‘ॐ’ को पृथ्वी की पहली ध्वनि मानता है। इसका निरंतर प्रयोग करने से शरीर, मन, आत्मा और आसपास के वातावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
मंत्र: हवन या यज्ञ में मंत्रों का विशेष स्थान है। मंत्र वे शब्द है जिसके द्वारा विश्व से संपर्क स्थापित किया जाता है। यह सेतु का कार्य करते हैं, जिसके बाद फिर मंगल कामना कर सकते हैं।
यज्ञ और हवन में अंतर
यज्ञ कुंड में अग्नि के माध्यम से देवता को प्रसाद या पदार्थ पहुंचाने की प्रक्रिया है- यज्ञ। जिसकी अग्नि में आहुति दी जाती है उन पदार्थों को हवि, हव्य या हविष्य कहते हैं, इससे हवन नाम पड़ा। हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित कर जिन पदार्थों की आहुति दी जाती है उनमें फल, शहद, घी, लकड़ी प्रमुख हैं। इस कर्मकांड को ही हवन कहते हैं।
यज्ञ और हवन को आज भी उतना ही शुभ और फलदायी माना जाता है जितना पहले माना जाता था। हवन और यज्ञ के बीच के अंतर को निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर समझा जा सकता है:
-हवन, यज्ञ का का ही छोटा रूप है। पूजा के बाद अग्नि में दी जाने वाली आहुति को हवन कहा जाता है। इसी तरह यज्ञ किसी विशेष उद्देश्य से देवता विशेष को दी गई आहूति है।
-कुंड में अग्नि के माध्यम से देवता के निकट भोजन पहुंचाने की प्रक्रिया हवन है, जबकि यज्ञ में देवता, आहूति, वेद मंत्र और दक्षिणा होना अनिवार्य है।
-हवन को हिंदू धर्म में शुद्धिकरण का कर्मकांड माना गया है, जबकि यज्ञ किसी विशेष उद्देश्य जैसे-मनोकामना की पूर्ति और अनिष्ट को टालने के लिए किया जाता है।
-हवन के माध्यम से आसपास की बुरी आत्माओं के प्रभाव को समाप्त किया जाता है, यज्ञ काफी बड़े पैमाने पर विशेष उद्देश्यों के लिए किया जाता है।
यज्ञ का इतिहास
प्रारंभ में यज्ञ का प्रमुख उद्देश्य समान विचार के अनेक लोगों का एकत्रीकरण रहा है। जब अग्नि का प्रयोग शुरू हुआ होगा तो आग के चारों ओर मानव गर्माहट के लिए बैठने लगा होगा। अन्न और भोजन को भुनने के लिए भी वह अग्नि के चारों तरफ इकट्ठा होता होगा। यह उनके सामाजिक मेलजोल का एक कारण बन गया होगा। जानवरों से सुरक्षा और ठंड से बचाव भी उनके एकत्र होने का कारण होता होगा। अग्नि से लेकर यज्ञ के वैदिक स्वरूप तक पहुंचने में इसने लंबा सफर तय किया होगा। उसमें अध्यात्म और प्रकृति का शुद्धिकरण जैसे अनुभव धीरे-धीरे मिले होंगे। एक जगह एकत्र होने के कारण अग्नि ‘देव’ बने रहे। आज भी होली और लोहड़ी जैसे त्योहारों पर अग्नि की भागीदारी को समझा जा सकता है।
वर्तमान युग में मनुष्य ने अपने आप को अकेला कर लिया है। जीवन में अकेलापन सामाजिक रोग बन गया है, जो कई तरह की बीमारियों का कारण है। ऐसे में सनातन संस्कृति का यज्ञ संस्कार लोगों को एक साथ लाने एवं एक जगह एकत्र करने का कारण बन सकता है। यज्ञ में ध्यान व प्रार्थना के द्वारा देवी शक्तियों का आव्हान करते हैं, जिसका प्रयोग हमारे पूर्वज वैदिक काल से करते आ रहे हैं।